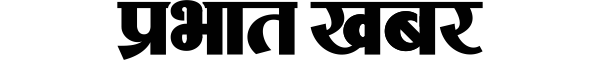प्रतिनिधित्व के खिलाफ खतरनाक मुहिम
।। उर्मिलेश ।। वरिष्ठ पत्रकार श्री श्री रविशंकर और पृथ्वीराज के बयानों से शुरू हुई मुहिम के खतरनाक पहलू के पीछे देश के दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के जन-प्रतिनिधित्व को भारतीय संसद में सीमित करने का मंसूबा साफ झलकता है. पिछले सप्ताह देश के दो जाने-माने लोगों ने संसदीय जन-प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की […]
।। उर्मिलेश ।।
वरिष्ठ पत्रकार
श्री श्री रविशंकर और पृथ्वीराज के बयानों से शुरू हुई मुहिम के खतरनाक पहलू के पीछे देश के दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के जन-प्रतिनिधित्व को भारतीय संसद में सीमित करने का मंसूबा साफ झलकता है.
पिछले सप्ताह देश के दो जाने-माने लोगों ने संसदीय जन-प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की वकालत की. उन्होंने अलग-अलग मौके पर कहा कि संसदीय चुनावों में सिर्फ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए, क्षेत्रीय दलों को नहीं. क्षेत्रीय दलों को सिर्फ उनके राज्य या क्षेत्र के प्रांतीय चुनावों तक सीमित कर देना चाहिए. इससे लोकतंत्र का स्वरूप बेहतर होगा और गठबंधन की मजबूरी खत्म होगी. अपने सुझाव के पक्ष में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने कई दलीलें दीं. रविशंकर शहरी मध्यवर्ग में लोकप्रिय गुरु माने जाते हैं.
कॉरपोरेट जगत में भी उनकी पकड़ बतायी जाती है. इस चुनाव में भाजपा ने उनकी सिफारिश पर कुछेक संसदीय क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का भी चयन किया. पृथ्वीराज मुख्यमंत्री होने के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस तरह की दो बड़ी शख्सीयतों ने संसदीय चुनाव की जारी प्रक्रिया के दौरान क्षेत्रीय दलों को ऐसे चुनावों से बाहर रखने का सुझाव क्यों दिया? दिलचस्प है कि इन दिनों कांग्रेस और भाजपा, दोनों चुनाव बाद के सत्ता-गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों को पटाने में जुटी हैं. पर रविशंकर और चह्वाण के बयान को लेकर दोनों ने चुप्पी साध ली है. इनका यह रहस्यमय रवैया उस बड़े खतरे का संकेत है, जो हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप ही नहीं, जन-प्रतिनिधित्व प्रक्रिया को भी संकट में डाल सकता है, क्योंकि इसके निशाने पर समाज के वंचित और उत्पीड़ित तबके हैं.
चह्वाण ने यहां तक कहा कि भारत को जर्मनी का मॉडल अपनाना चाहिए, जहां क्षेत्रीय दलों-समूहों को केंद्रीय चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है. उनके मुताबिक ऐसा करने से केंद्र में स्थिरता रहेगी. अगर उनका सुझाव मान लिया जाये, तो संसदीय चुनाव में उतरने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस, भाजपा, बसपा, भाकपा, माकपा और एनसीपी को होगा. अन्य सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस अधिकार से वंचित हो जायेंगे. बहुत संभव है, आम चुनाव के बाद भाकपा और एनसीपी भी राष्ट्रीय दलों की सूची से बाहर हो जायें. यानी देश की सबसे पुरानी वामपंथी पार्टी को भी संसद में अपना जन-प्रतिनिधि भेजने की इजाजत नहीं मिलेगी.
यह किसका एजेंडा हो सकता है? ऐसे बदलाव से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर? राष्ट्रीय एकता-अखंडता को ताकत मिलेगी या उसमें दरार आयेगी? इससे केंद्र की सरकारें ज्यादा सक्षम, समर्थ और स्थिर होंगी या बेलगाम और निरंकुश होती जायेंगी? हमारे लोकतंत्र में जन-हिस्सेदारी बढ़ेगी या सिकुड़ेगी? ऐसे अनेक सवाल रविशंकर और चह्वाण के सुझावों के संदर्भ में स्वाभाविक तौर पर उठते हैं.
पहले भी इस तरह की मंशा भाजपा-आरएसएस से जुड़े कुछ ‘विचारकों’ ने समय-समय पर जाहिर की है. एनडीए सरकार के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी की खास पहल पर संविधान में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए संविधान-समीक्षा का एक प्रयास भी शुरू हुआ था. लेकिन 2004 के चुनाव में एनडीए सरकार के पतन के बाद वह स्वत: ही खत्म हो गया. क्या इस बार फिर भाजपा के एजेंडे में यह मुद्दा शामिल है? जाहिर है, ऐसी चीजें घोषणापत्र में शामिल करके अमल में नहीं लायी जातीं.
कुछ वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जरिये देश में दो-दलीय व्यवस्था का एक सुझाव चर्चा में लाने की कोशिश की गयी. क्या भाजपा-कांग्रेस के बीच इस दिशा में कुछ सहमति बनी है और रविशंकर एवं चह्वाण के बयान उस सहमति की अभिव्यक्ति भर हैं? यह शंका या अटकल का प्रश्न नहीं है. दोनों पार्टियों में किसी ने भी इस सुझाव को पूरी तरह नकारता हुआ बयान नहीं जारी किया.
कुलीन मानसिकता के कुछ ‘विचारकों’ ने तो पिछले दिनों यहां तक कहा कि संसदीय चुनावों में मतदान का अधिकार सीमित किया जाना चाहिए. सिर्फ पढ़े-लिखे या कम-से-कम स्नातक स्तर की शिक्षा हासिल कर चुके लोगों को ही मताधिकार मिले. इससे लोकतंत्र और संसदीय चयन की गुणवत्ता बढ़ेगी. वस्तुत: विविधता भरे हमारे समाज में ऐसा सोच लोकतंत्र के खिलाफ एक खतरनाक मुहिम का संकेत है.
इस तरह के ‘विचारकों’ ने अपने फूहड़ सोच और खतरनाक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मध्यवर्गीय भारत के बड़े हिस्से में इस बात का जोरदार प्रचार किया है कि 1989 के बाद लंबे समय तक केंद्र में सरकारों की स्थिरता सिर्फ क्षेत्रीय दलों या नेताओं के चलते प्रभावित होती रही. अच्छी सरकार का मतलब एक स्थिर और मजबूत सरकार है या कि अच्छी सरकार सिर्फ कांग्रेस या भाजपा दे सकती है. दूसरे दलों या गंठबंधनों के लिए अच्छी सरकार देना संभव ही नहीं है. इस ‘झूठ’ को प्रचारित करने में मीडिया के एक हिस्से की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है. आज देश का बड़ा कॉरपोरेट वर्ग भी यही चाहता है, इसलिए मुख्यधारा मीडिया का बड़ा हिस्सा भला कैसे अलग सुर में बोले! पर कौन नहीं जानता कि 1979 से लेकर आज तक केंद्र की गठबंधन सरकारें किसके इशारे या साजिशों पर गिरायी गयीं? मोरारजी, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा या गुजराल, इन सबकी सरकारें किनकी मुहिम का शिकार हुईं? हर बार, राष्ट्रीय दलों- कांग्रेस-भाजपा या संघ परिवारी शक्तियों ने ही गंठबंधन की सरकारों को संकट में डाला. क्या यह सच नहीं कि इस देश में सबसे बेहतर बदलाव, सुशासन या कामकाजी माहौल बनाने की कामयाब कोशिश राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों की पहल पर ही हुई? कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, केरल में इएमएस, पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और कर्नाटक में देवराज अर्स के अपने प्रयासों से ही भूमि-सुधार जैसा जरूरी एजेंडा कारगर ढंग से लागू किया जा सका. आज भी क्षेत्रीय दलों के कई मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में सरकार चला रहे हैं. राष्ट्रीय दलों से जुड़े अतीत के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले वे अपने सूबे में ज्यादा कामयाब माने जा रहे हैं.
श्री श्री रविशंकर और पृथ्वीराज चह्वाण के बयानों से शुरू हुई मुहिम के खतरनाक पहलू के पीछे देश के दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के जन-प्रतिनिधित्व को भारतीय संसद में सीमित करने का मंसूबा साफ झलकता है. सवर्ण-सर्वसत्तावाद की यह सबसे भौड़ी अभिव्यक्ति है. इस बात में शायद ही किसी को शक हो कि समाज के उत्पीड़ित वर्गो का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आज क्षेत्रीय दल ही कर रहे हैं. हालांकि ऐसे दलों की अपनी-अपनी समस्याएं भी हैं. उनमें कहीं परिवारवाद, तो कहीं संकीर्णतावाद भी पनप रहा है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें संसद से बाहर रखा जाये. क्या राष्ट्रीय दल इस तरह की व्याधियों से मुक्त हैं?