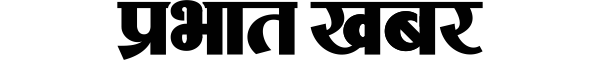किसानी से डरने वाला समाज
IIमृणाल पाण्डेII ग्रुप सीनियर एडिटोरियल एडवाइजर, नेशनल हेराल्ड mrinal.pande@gmail.com आज के भारत भाग्य विधाता मानें या नहीं, अन्न उत्पादन के मामले में भारत का आत्मनिर्भर बन जाना, बीसवीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं और हमारी राष्ट्रीय उपलब्धियों में से है. लेकिन, कम लोगों को याद होगा कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने नोबेल […]
IIमृणाल पाण्डेII
ग्रुप सीनियर एडिटोरियल एडवाइजर, नेशनल हेराल्ड
mrinal.pande@gmail.com
आज के भारत भाग्य विधाता मानें या नहीं, अन्न उत्पादन के मामले में भारत का आत्मनिर्भर बन जाना, बीसवीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं और हमारी राष्ट्रीय उपलब्धियों में से है. लेकिन, कम लोगों को याद होगा कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते वक्त भाषण में दो बातें कही थीं. पहला, हरित क्रांति अमरता की बूंदें पी कर नहीं आयी. इसका भी किसी दिन अंत होगा और इसलिए अभी उसे लागू करने लायक ढांचा तैयार करना होगा. दूसरा, सरकारों ने इसे सफलता से लागू करा लिया, तो उसके बाद भी उनको अतिरिक्त अन्न और फल-साग की बर्बादी रोकने को अन्नभंडारण गोदाम, फसलों के न्यूनतम दाम और मुनाफाखोर बिचौलियों द्वारा जबरन पैदा की गयी अन्न की नकली कमी जैसे सरदर्दों से निबटना होगा. इसके लिए जरूरी है कि वे पहली सफलता पर अपनी पीठ थपथपा कर आरामतलब न बनें, लगातार कृषि वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों, बाजार के विशेषज्ञों से संपर्क रखें और उनसे विमर्श व मदद लेते रहें.
बोरलॉग ने दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि मानवता दो परस्पर विरोधी धाराओं से घिरी हुई है. विज्ञान ने एक तरफ हमें अन्न-उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी की ताकत दी है, पर दूसरी तरफ संतानोत्पत्ति की बेहिसाब संभावना को बेहतर खानपान व चिकित्सा पद्धतियों ने बढ़ावा दिया है. इसलिए सभी देशों को अधिक अन्न-उत्पादन के साथ आबादी नियंत्रण पर भी काम करना होगा. आबादी नियंत्रित नहीं हुई, तो गांवों में जोत लगातार कम होगी और पलायन से शहर तकलीफदेह तौर से असंतुलित होने लगेंगे. यह न हो, तो इसके लिए सरकारों को जमीन, समाज और घरेलू उपभोक्ता वर्ग को नजर में रखते हुए समुन्नत कृषि के लिए लगातार समयानुकूल प्रयास करने होंगे और सिंचाई के लिए मानव निर्मित सिंचाई का रकबा बढ़ाना होगा.
वर्ष 1971 के इस अविस्मरणीय भाषण के चार दशक बाद सदियों से अन्न के अभाव के साये में जीते रहे हमारे देश को अन्न की विपुलता के साथ उससे उपजने जा रहे नये सरदर्दों से जूझना पड़ रहा है. पैदावार बढ़ी, तो फसलों के भाव कम हुए, लेकिन महंगे बीज, पंप और उर्वरक का इस्तेमाल करने से किसानी की लागत बढ़ने के साथ पानी और बिजली की खपत भी बढ़ी. ऐसे में किसानी को लाभकारी और समृद्धि का स्रोत बनाये रखने और किसानों के वोट पाने के दो ही रास्ते पार्टियों को दिखे- एक सरकारें निर्यात के लिए नये बाजार खोजें, और जरूरत के मुताबिक सब्सिडी देकर अन्न के भाव इतने ऊंचे रखें कि किसानों और मंडियों का दिवाला न निकले और कृषि की आय को करमुक्त रखा जाये. पर इससे फायदा हुआ बड़े जोतदारों को. मुफ्त बिजली पानी के बूते वे पूंजीपति बने और बाजारों, मंडियों व सहकारी ग्रामीण बैंक के लोन तक पर कब्जा करने लगे. उधर, सामान्य किसान के परिवार बढ़े, जोत कम हुई और खेती का खर्च बढ़ता गया.
गांव के खानदानी किसानों का हर हुनर किसानी से ही जुड़ा होता है. शहरी कामों लायक कोई हुनर उसके पास नहीं होता. कोई हस्तशिल्पकार या कारीगर गांव छोड़ कर शहर में चार रोटी भले से कमा भी ले, पर छोटे किसान जमीन छोड़ कर कहां जायेंगे, कैसे जियेंगे?
वर्ष 2018 तक अन्नक्रांति के असंख्य नये आर्थिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय नतीजे सामने आ चुके हैं. जब राजनेता और बड़े किसानों की बेईमानी से सहकारी बैंक दिवालिया होने की कगार पर आ गये, तो संपन्न राज्यों के गांव में राजनेताओं के प्रोत्साहन से सरकारी बैंकों ने प्रवेश किया. कृषि बीमा का नया नारा आया, जिसके लिए जीरो पैसेवाले किसानी खाते खुले, जिनमें सरकार द्वारा बीमा राशि भेजी जानी थी. बीमा कंपनियां आयीं और सरकारी सब्सिडी से उन्हें हिस्सा भी मिल गया. पर जहां तक किसान का अनुभव है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से बड़ी तादाद में वे बारिश पर निर्भर हैं. अत: भारत में फसल का बीमा करने का मतलब है, मौसम का बीमा. चार बरस सुखाड़, दो बरस बाढ़, कभी अंधड़ तो कभी ओले. मौसम अनिश्चित बनता गया, तो किसान के लिए समय पर बैंक से लिया लोन चुकाना हलक का कांटा बन गया.
खेती राज्यों का विषय है, इसलिए केंद्र राज्यों को योजनावार सुझाव दे सकता है, राजकोषीय घाटे का खतरा मोल लेकर चुनाव पास आने पर कई बार राज्य विशेष को अतिरिक्त राशि भी मुहैया करा देता है, पर सच यह है कि कृषि योजनाओं को राज्य सरकारों को ही संचालित करना होता है. चुनाव-दर-चुनाव जाति, धर्म और शहर बनाम गांव के आधार पर वोट लेने की वजह से विकास का कोई सही दूरगामी खाका नहीं बन सका है. लिहाजा राज्य अपने कराधान का 85 फीसदी हिस्सा तनख्वाह, पेंशन और किसानी बैंक लोन व बिजली सब्सिडी के बिल भरने में खपाते रहने को मजबूर हैं, ताकि किसानी वोट बैंक खुश रहे. पर अब शहरी वोट बैंक बढ़ा है. शहरियों का सरकार पर दबाव है कि अनाज महंगा न हो, गांवों की जमीन पर नये औद्योगिक उपक्रम खुलते रहें, उनके घर में पानी-बिजली की कमी न हो.
हरित क्रांति के बाद शहरों के खानपान के तरीके बदले हैं. अन्न की मांग घटी और फलों-सब्जियों, अंडा-मांस, दूध की खपत बढ़ी है. इससे किसान अधिक पशुपालन और फल-सब्जी उगाने लगे. लेकिन भंडारण और शहरों तक माल ढुलाई की व्यवस्था में कोई खास तरक्की नहीं हुई और न ही कृषि उत्पाद मार्केट कमेटियां बिचौलियों के उन गुप्त परिसंघों पर रोक लगा पायी हैं, जो हर बार सीजन आने पर दाम क्रैश करा देते हैं. दूसरी ओर, दक्षिणपंथी दलों द्वारा मांस की बिक्री व पशुओं की खरीद-फरोख्त में टांग अड़ाने से खेती और पशुपालन पर समवेत रूप से निर्भर छोटे किसानों की मिट्टी पलीद हो रही है.
देश के कृषि मंत्री या कोई मुख्यमंत्री भले ही पशु विक्रेताओं को शक की बिना पर सड़कों पर मारने या मुंबई से मंदसौर तक फैल रहे किसान आंदोलनों को छोटे किसानों का विपक्ष द्वारा प्रायोजित नाटक मात्र बतायें, पर खतरा बहुत बड़ा, देशव्यापी और बहुमुखी बनता चला गया है और सब्सिडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी, पेट्रोलियम उत्पादों पर चंद पैसे कम करने या दालें आयात करने के पुराने हथियारों-वादों से यह नित नयी चुनौतियां बहुत दूर तक नहीं निबटायी जा सकेंगी.