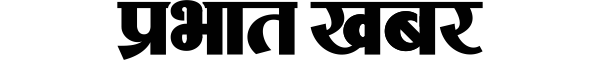बैंक पूंजी में बढ़त
बीते कुछ सालों से सार्वजनिक बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को संतोषजनक बनाये रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है. भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और निकट भविष्य में डूबे कर्जों की वसूली की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है. ऐसे कर्जों की मात्रा बैंकों की […]
बीते कुछ सालों से सार्वजनिक बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को संतोषजनक बनाये रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है. भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और निकट भविष्य में डूबे कर्जों की वसूली की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है. ऐसे कर्जों की मात्रा बैंकों की कुल परिसंपत्ति का 13 फीसदी तक जा पहुंची है, जो करीब तीन साल पहले तक तीन फीसदी से भी कम थी.
इस कारण बैंकों के पास कर्ज देने के लिए धन की कमी होना स्वाभाविक ही है. अर्थव्यवस्था की तेजी को बरकरार रखने के लिए उद्यमों और परियोजनाओं के लिए कर्ज की उपलब्धता जरूरी है. इस संकट से बैंकों को उबारने के लिए सरकार ने ढाई लाख करोड़ रुपये देने का भरोसा दिया था. अक्तूबर, 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2.11 लाख करोड़ मुहैया कराने की योजना की घोषणा की थी. इससे पहले भी कुछ राशि बैंकों को मिली थी.
इसमें 1.35 लाख करोड़ बॉन्ड से, 58 हजार करोड़ बाजार से और शेष बजट सहयोग से उपलब्ध होना था. पिछले डेढ़ साल में सरकार ने 1.95 लाख करोड़ रुपये बैंकों को दे दिया है. वित्त वर्ष 2017-18 में 88 हजार करोड़ और 2018-19 में 65 हजार करोड़ रुपये बैंकों को मिले थे. बैंक बाजार से पैसा लाने में कामयाब नहीं हो सके, तो सरकार ने फिर 41 हजार करोड़ रुपया दिया है.
बैंकों की इस मदद की जरूरत इसलिए भी थी कि वे रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन करते हुए कर्ज दे सकें. केंद्रीय बैंक के नियम के अनुसार, एक निश्चित वित्तीय क्षमता होने के बाद ही बैंक नये कर्ज दे सकते हैं. सरकारी सहायता के बाद अनेक बैंक इस शर्त को पूरा कर सकते हैं और कुछ बैंक उस स्तर से नीचे आने से बच सकते हैं. रिजर्व बैंक और सरकार ने फंसे कर्जों की वसूली और नये कर्जों को इस श्रेणी में जाने से रोकने के लिए मजबूत पहलकदमी की है. पूंजी की उपलब्धता जहां अर्थव्यवस्था के लिए मददगार होगी, वहीं इससे बैंकों की क्षमता भी बढ़ेगी.
यह उम्मीद भी है कि उन्हें अतिरिक्त धन की जरूरत नहीं पड़ेगी. रिपोर्टों की मानें, तो सरकार भी अगले वित्त वर्ष में पूंजी नहीं देगी और उसे अपेक्षा है कि तीन-चार बड़े बैंक बाजार से धन जुटा सकेंगे. पूंजी देने से जहां बैंकों की हालत बेहतर हो रही है, वहीं इससे डिजिटल लेन-देन, वित्तीय समावेश की योजनाओं तथा किसानों के क्रेडिट कार्ड में भी फायदा होने की उम्मीद है. इस जरूरी पहल के साथ बैंकिंग सेक्टर की बेहतरी के लिए अन्य उपायों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या का एक मुख्य कारण बैंकों के प्रबंधन और निगरानी की खामियां हैं. रिजर्व बैंक को इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों को तेज करना चाहिए. आपसी विलय के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम करने की प्रक्रिया भी सराहनीय है. आशा है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ बैंकों की स्थिति में भी लगातार सुधार होगा.