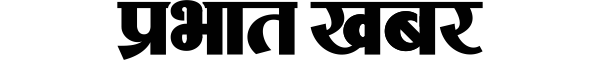भारत के लिए ली कुआन यू आदर्श नहीं
आकार पटेल वरिष्ठ पत्रकार सिर्फ एक मजबूत नेता को लाने से स्थिति नहीं बदल सकती, और मुङो ऐसा नहीं लगता कि ली ने इसे पूरी तरह से समझा होगा, जब वे अकसर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि उनकी महान सफलताएं भारत जैसे देशों में क्यों दुहरायी नहीं जा सकीं. सिंगापुर के महान नेता ली कुआन […]
आकार पटेल
वरिष्ठ पत्रकार
सिर्फ एक मजबूत नेता को लाने से स्थिति नहीं बदल सकती, और मुङो ऐसा नहीं लगता कि ली ने इसे पूरी तरह से समझा होगा, जब वे अकसर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि उनकी महान सफलताएं भारत जैसे देशों में क्यों दुहरायी नहीं जा सकीं.
सिंगापुर के महान नेता ली कुआन यू की मृत्यु पर उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने उनकी आर्थिक उपलब्धियों को रेखांकित किया- ‘ली और इनके सहयोगियों ने अपने लोगों की प्रतिव्यक्ति आय, जो आजादी के बाद 1965 में 500 डॉलर थी, को वर्तमान में करीब 55,000 डॉलर तक पहुंचा दिया. एक पीढ़ी की अवधि में ही सिंगापुर एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रमुख बौद्धिक महानगर, क्षेत्र के बड़े अस्पतालों का स्थान और अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबद्ध सम्मेलनों की पसंदीदा जगह बन गया.’
यह एक असाधारण उपलब्धि है और ऐसी तीव्र वृद्धि इतिहास में कुछ ही देशों द्वारा दुहरायी जा सकी है. हालांकि, यह नहीं भूला जाना चाहिए कि ली कुआन यू को सिंगापुर कुछ अनुकूल परिस्थितियों के साथ मिला था. उस पर एक शताब्दी से अधिक समय तक ब्रिटिश शासन रहा था, वह अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह था, और आजादी के समय तक वह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था.
सिंगापुर की आय को संदर्भो से समझने की कोशिश करते हैं. वर्ष 1965 में आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बहुत अधिक विषम समाजवाले देश भारत में प्रति व्यक्ति आय 100 डॉलर थी. एक अन्य सकारात्मक बात सिंगापुर के साथ यह थी कि वह बहुत कम जनसंख्या के साथ बहुत छोटा देश था. आबादी का दो-तिहाई या इससे अधिक हिस्सा उद्यमी चीनी आप्रवासियों का है, जिनके कंफ्यूसियन संस्कार अधिनायकवाद के प्रति समर्पण के लिए अभ्यस्त होते हैं.
ली का अनुशासित और ईमानदार प्रशासन इन अनुकूलताओं को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सका और उन्होंने सही मायनों में एक वैश्विक शहर बनाया. सिंगापुर जानेवाला कोई भी व्यक्ति उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता है. जापान से यूरोप तक कोई शहर इससे अधिक समृद्ध और स्वच्छ नहीं है और न ही उसके प्रशासन से बेहतर है. इसमें किसी को संदेह नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि वे ‘एक दूरदर्शी राजनेता और नेताओं में सिंह थे. ली कुआन का जीवन हर किसी को अमूल्य पाठ की सीख देता है.’ लेकिन, ये पाठ कौन-से हैं और क्या उन्हें भारत जैसे देशों पर लागू किया जा सकता है? मोदी जैसे मजबूत नेता (और किसिंजर जैसे मजबूत नेता भी, जिनके पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे) ली को इसलिए पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता लगभग निरंकुश थी. ऐसा होने के लाभ क्या थे?
मुङो एक पत्र का अंश उद्धृत करने की अनुमति दें, जिसे एक 46 वर्षीय प्रबंधक ली केक शिन ने सिंगापुर के प्रमुख समाचार-पत्र ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ को 2012 में लिखा था. इस पाठक ने अखबार में छपे एक लेख ‘द्विदलीय व्यवस्था यहां व्यावहारिक नहीं’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था, ‘प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग सोचते हैं कि यहां दो अच्छे राजनीतिक दल बनाने के लिए प्रतिभाओं का अभाव है, लेकिन मामला इससे कहीं अधिक है. हम ऐसे दो देशों- जैसे, भारत और चीन- के बीच तुलना करें, जहां एक में बहुदलीय व्यवस्था है और दूसरे में एक दलीय शासन. दोनों देशों में वृहत जनसंख्या है और आम तौर पर एक समान संस्कृति है. हालांकि दोनों देश अच्छी आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि चीन का प्रदर्शन बेहतर है.’
मेरी राय में इसका श्रेय चीन के एककदलीय राज्य (भले ही वह कम्युनिस्ट हो) को दिया जा सकता है. एक ही दल का होना देश को एक दिशा में ले जाने के लिए नेताओं को गुंजाइश देता है. दूसरी ओर, द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था में हर पार्टी अपने हितों को साधने में लगी रहती है, जो कभी-कभी देश की प्रगति की कीमत पर होता है. उदाहरण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से देश को फायदा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी योजना दलगत विरोध से बाधित भी हो सकती है.
अकसर ही कोई देश आर्थिक रूप से पीछे की ओर जाने लगता है, जैसे कि अमेरिका, जहां पिछले एक दशक से प्रगति में ठहराव है, क्योंकि एक राजनीतिक दल दूसरे दल को पछाड़ने की जुगत में रहता है. प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई शक्तियों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं.
लेकिन, सिंगापुर के साथ खास बात यह भी रही कि यह कुछ वर्ष पूर्व आये वित्तीय संकट से प्रभावित हुए बिना निकल आया. मेरा मानना है कि ऐसा हमारी एकदलीय सरकार द्वारा देश को एक दिशा में संचालित करने के कारण हो सका. द्विदलीय या बहुदलीय व्यवस्था वाले बड़े देश गलतियां करना और फिर उबरना गंवारा कर सकते हैं, लेकिन सिंगापुर जैसे छोटे देश के लिए दूसरे मौके की कोई जगह नहीं है.’
ली की सफलता के पक्ष में यह एक जोरदार तर्क है : सिंगापुर पर उनकी तानाशाही. आबादी में निहित प्रतिभा और राज्य के आकार के ऐसी तानाशाही के अनुकूल होने के तथ्य को शायद ही कभी चिह्न्ति किया गया है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए राज्य का गहरा प्रभाव जरूरी है.
हालांकि, राज्य की दखल की समस्या (जिसका अर्थ हिंसा पर एकाधिकार, नागरिकों को स्वेच्छा से कराधान पर राजी करना, न्याय और सार्वजनिक यातायात जैसे बुनियादी सेवाओं का निष्पादन) का समाधान भारत जैसे विशाल, अव्यवस्थित और संसाधन की कमी से जूझते देश में आसानी से नहीं किया जा सकता है. सिर्फ एक मजबूत नेता को लाने से स्थिति नहीं बदल सकती, और मुङो ऐसा नहीं लगता कि ली ने इसे पूरी तरह से समझा होगा, जब वे अकसर आश्चर्य व्यक्त करते थे कि उनकी महान सफलताएं भारत जैसे देशों में क्यों दुहरायी नहीं जा सकीं.
इस तंत्र से हुए नुकसान को भी नजरअंदाज किया गया है. ऑस्ट्रेलिया चले गये मेरे सिंगापुरी मित्र पीटर ओंग ने उस कठोरता को पसंद नहीं किया, जिसके द्वारा सिंगापुर में नागरिकों पर एकरूपता थोपी गयी.
ली की मनमानी और सनक-भरे कानूनों (जैसे- च्यूविंग गम पर पाबंदी और बेंत मारने का शारीरिक दंड लागू करना) ने देश की छवि को धूमिल ही किया. नागरिकों की आय में भारत से 30 गुना वृद्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर सिंगापुर को आदर्श के रूप में देखना सही नहीं होगा. और यह भी मानना ठीक नहीं होगा कि वे या उनके जैसा कोई मसीहाई व्यक्ति भारत जैसी जगह में ऐसा कर पाता.