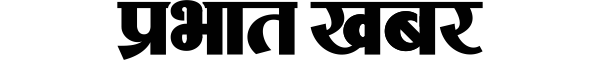भारतीय ज्ञान परंपरा और चीन
डॉ देवेंद्र शुक्ल पेकिंग विवि में प्रोफेसर रहे हैं. अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष हैं. देश की उपयोगिता के अनुसार, अगर हम शिक्षा व्यवस्था का विकास करें, देशी भाषा को प्रश्रय दें, और अंगरेजी को सिर्फ लिंक लैंग्वेज तक सीमित रखें, तभी हम सही मायने में भारतीय शिक्षा का विकास कर […]
डॉ देवेंद्र शुक्ल
पेकिंग विवि में प्रोफेसर रहे हैं. अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष हैं.
देश की उपयोगिता के अनुसार, अगर हम शिक्षा व्यवस्था का विकास करें, देशी भाषा को प्रश्रय दें, और अंगरेजी को सिर्फ लिंक लैंग्वेज तक सीमित रखें, तभी हम सही मायने में भारतीय शिक्षा का विकास कर सकते हैं और चीन के बराबर खड़े हो सकते हैं.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा के दौरान जिस श्यान प्रांत में गये हैं, वह ह्वेनसांग की धरती है. आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन चीन के इस प्रांत से हमारा रिश्ता, या यूं कहें कि चीन की शिक्षा के हरेक क्षेत्र से हमारा रिश्ता प्राचीन काल से है.
चीन और भारत सदियों से ज्ञान-विज्ञान का आदान-प्रदान करते आये हैं. भारत के फूल चीन में मिलते हैं और वहां की आबोहवा भारत में. दोनों देशों के बीच अगर मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं, तो इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का अहम योगदान है.
भारत की ज्ञान परंपरा वैदिक ज्ञान पर आधारित है, जबकि चीन की ज्ञान परंपरा लाओत्से और कन्फ्यूशियस की परंपरा पर.
लाओत्से की परंपरा हमारे वैदिक ऋषियों के समकक्ष रही है, जहां सहजता से जुड़ने की बात की जाती थी, कृत्रिमता से नहीं. वहीं कन्फ्यूशियस की परंपरा मूल रूप से समाज और परिवार के साथ व्यवहार से जुड़ी है, अर्थात् मूल सिद्धांत आदर्श नहीं, बल्कि व्यवहार हो, ऐसी धारणा बनाती है. वर्तमान चीन इसी परंपरा को मानता है और इसे ही आगे बढ़ाता है.
हम वाचिक परंपरा से आगे बढ़े हैं, जबकि चीन लिखित परंपरा को अपनाता आया है. वहां 7000 ईसा पूर्व से ही स्क्रिप्ट (लिपिबद्धता) शुरू हो गयी थी, यानी ज्ञान-विज्ञान को लिपिबद्ध करना शुरू हो गया था. लेकिन, वाचिक परंपरा अपनाने के साथ ही हम प्रायोगिकता की दिशा में भी काम करते आये हैं.
प्लेटो के दर्शन पर भारतीय प्रभाव है. गणित, ज्योतिष विज्ञान पर प्राचीन विश्वविद्यालयों- नालंदा और तक्षशिला का प्रभाव है. हमारे यहां पारंपरिक शिक्षा के साथ वोकेशनल शिक्षा का भी प्रचलन रहा है. हमारे देश के विद्वान प्राचीन काल से ही चीन जाते रहे हैं.
चीन और भारत में शिक्षा के आदान-प्रदान का पहला श्रेय कश्यप मातंग को जाता है. ह्वेनसांग, जो कि 15 वर्ष तक भारत में रहे, ने नालंदा की सारी किताबें चीन पहुंचा दीं. न्याय, दर्शन, ज्योतिष और बौद्ध दर्शन की बहुत सारी किताबें जल गयीं. राहुल सांकृत्यायन ने 1,500 किताबों की सूची भारत सरकार को सौंपी है.
मैंने खुद भारत सरकार को प्राचीन समय की 500 किताबों की सूची सौंपी है. मतलब यह है कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था काफी समृद्ध रही है, जिस पर चीन का आज का वर्तमान विकसित हो रहा है. लेकिन, यह हमारी गलती है कि हम उस समृद्ध इतिहास को बरकरार नहीं रख पाये.
आज यदि हम चीन की शिक्षा व्यवस्था से कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसमें दो-तीन बातें प्रमुख हैं. चीन में थ्री-इडियट फिल्म पूरे साल दिखायी गयी. इससे यह जाहिर होता है, हम विश्वविद्यालयी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें करना क्या है? अर्थात् दिग्भ्रम की स्थिति होती है. जबकि चीन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है. वहां जैसे ही कोई छात्र हाइस्कूल की परीक्षा पास करता है, उसे एक टेस्ट से गुजरना होता है.
उसी के आधार पर उसकी आगे की शिक्षा होती है, ताकि वह शिक्षा को रोजगार का माध्यम बना सके. चीन में वोकेशनल शिक्षा काफी प्रचलन में है. वहां जोड़ने की कला काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. शिल्प, वास्तुकला आदि क्षेत्रों में चीन काफी आगे है. सूई से लेकर गणोश तक चीन में बनाये जाते हैं.
दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चीन अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति काफी उत्सुक रहता है, उसका सम्मान करता है और उसी पर काम करता रहता है. जबकि, हमारे यहां मातृभाषा को महत्व ही नहीं दिया जाता. आज हमारी पूरी ज्ञान प्रणाली अंगरेजी पर आधारित है, जिसकी वजह से हम उस गति से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, जितनी गति से होनी चाहिए.
चीन के सभी बड़े विश्वविद्यालय अलग-अलग विषयों की विशेषज्ञता के लिए अपनी पहचान रखते हैं, मसलन शिन्हुआ इंजीनियरिंग और गणित के लिए, पेकिंग आर्ट और कल्चर के लिए. इन सबके पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा रही है और इसी दौर में विश्वविद्यालयों का विकास हुआ. आज चीन इस दिशा में आगे बढ़ते हुए शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर चुका है.
कन्फ्यूशियस के चीन से मुकाबला करने के लिए, या यह कह सकते हैं कि उस रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए हमें इसी तरह की पहल करनी होगी. हमें यूजीसी के मानकों से आगे निकलते हुए नये मानक गढ़ने होंगे.
देश की उपयोगिता के अनुसार, अगर हम शिक्षा व्यवस्था का विकास करें, देशी भाषा को प्रश्रय दें, और अंगरेजी को सिर्फ लिंक लैंग्वेज तक सीमित रखें, तभी हम सही मायने में भारतीय शिक्षा का विकास कर सकते हैं और चीन के बराबर खड़े हो सकते हैं.
(संतोष कुमार सिंह से बातचीत पर आधारित)