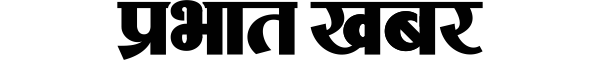अंगरेजी के आतंक से मुक्ति कब!
।।नंद चतुव्रेदी।।(वरिष्ठ साहित्यकार)(शनिवार के अंक से आगे)बौद्धिकों का ‘प्रभु वर्ग’ मैकॉले के हस्तक्षेप से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी स्थापनाओं का मुखर प्रचारक हो गया. वह इस प्रचार में लग गया कि अंगरेजी राज न आया होता और अंगरेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान व रोशनी न फैली होती, तो भारतीय समाज कभी अपने सामंती […]
।।नंद चतुव्रेदी।।
(वरिष्ठ साहित्यकार)
(शनिवार के अंक से आगे)
बौद्धिकों का ‘प्रभु वर्ग’ मैकॉले के हस्तक्षेप से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी स्थापनाओं का मुखर प्रचारक हो गया. वह इस प्रचार में लग गया कि अंगरेजी राज न आया होता और अंगरेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान व रोशनी न फैली होती, तो भारतीय समाज कभी अपने सामंती अंधेरों से मुक्त न हो पाता. यह ‘वर्ग’ यह भी प्रचार करने लगा कि अंगरेजों की कृपा से रेल, डाक, न्याय-व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, अखबार व अन्य साधनों से देश का आधुनिकीकरण संभव हुआ. किंचित अचरज की बात यह भी थी कि इस प्रगति को अंगरेजी के साथ जोड़ कर देखा जाने लगा. एक खास वर्ग के लोग इंग्लैंड जाकर शिक्षित होने के साथ भारत में ऊंचे-ऊंचे प्रशासनिक पद पाने लगे. इससे अंगरेजी हुकूमत को दो लाभ हुए. एक तो यह कि उन्हें इंग्लैंड से महंगे अधिकारी नहीं लाने पड़े, यहीं देसी, चतुर व अपेक्षाकृत सस्ते अधिकारी मिल गये. दूसरा यह कि वे अधिक स्वामीभक्त साबित हुए. वे मैकॉले की उस स्थापना के अनुकूल थे, जो यह मांग करती थी कि ‘केवल रक्त और रंग से हिंदुस्तानी रह जायें, बाकी सब तरह के विवेक, विचार, बौद्धिक-प्रखरता, नैतिक निष्ठाओं से अंगरेज.’ ध्यान से देखें तो वे अधिक ऊर्जा व उग्रता से अंगरेजीराज के प्रचारक हो गये.
देखते-देखते देशी भाषाओं की पढ़ाई और देशी ज्ञान-मीमांसा की गरिमा सहज ही समाप्त हो गयी. दरअसल वह पहले से ही अव्यवस्थित और बिखरी हुई थी. निरंतर होनेवाले आक्रमणों, जाति-व्यवस्था की अहंकारी भावना और सामंती लालसाओं की राजनीति से आहत देश में शिक्षा या भाषा का कोई रूप बचा भी नहीं सकता था, तब सहसा एक सुनियोजित शिक्षा का संकल्प बरबादी बचानेवाला लगा. यह बात अलग है कि उस ‘विकल्पहीनता’ ने ऐसी निराशा की जमीन तैयार कर दी, जिसमें फिर दूसरी कोई फसल उगाना मुश्किल हो गया.
धीरे-धीरे शिक्षा के सामंतों को पार करता हुआ संपूर्ण शासन-तंत्र अंगरेजी भाषा के दबाव में आ गया. जिस ‘क्लास’ की बात मैकॉले कर रहे थे, उसके बनने में ज्यादा देर नहीं लगी. यह जमात बाबू कहलाने लगी. उस समय की कहानियों के चरितनायक ‘बड़े बाबू’ ‘छोटे बाबू’ की तरह पहचाने जाने लगे. उनकी वेशभूषा, बोल-चाल, रहन-सहन, आचरण-अंदाज, सामान्य भारतीय गृहस्थ से सर्वथा अलग नजर आने लगे. इतने अलग और आतंककारी, कि ब्रजभाषा के एक कवि ने लिखा ‘हाबू ज्यों डरात, देशवासिन को जाबू फाड़ काबू में न आवे बात बाबू के दिमाग की’. (बाबू के दिमाग की बात हमारे समझ में नहीं आती, वह हमें किसी डरावने कीड़े की तरह आतंकित करती हैं).
बाबुओं की इस देशज-जमात को यह आर्थिक-बदलाव इतना पसंद आया कि वे इस व्यवस्था के दीर्घकालीन प्रभावों, बरबादियों, पराधीनता और शोषण को भूल कर अंगरेज-बहादुरों का कीर्तन करने लगे. देखते-देखते और चुपचाप न्यायालयों, कोर्ट-कचहरियों, पोस्ट-टेलीग्राफ ऑफिसों तथा सार्वजनिक दफ्तरों का काम अंगरेजी भाषा में होने लगा. भारतीय भाषाओं को ‘वर्नाक्युलर लेंग्वेजेज’ कह कर दोयम दरजे के भाषा खांचे में डाल दिया गया, जिन्हें अंगरेजी के मुकाबले में आज तक गरिमामय स्थान नहीं मिला. देखने की बात यह है कि ज्यों-ज्यों अंगरेजी भाषा का दायरा फैलता गया, शासक वर्ग और जनता के बीच का फासला चौड़ा होता गया. एक संवादहीनता की स्थिति बनती गयी, जो अंत में अविश्वसनीयता और आतंक में बदल गयी. एक तरफ अंगरेजी कवियों, लेखकों और उपन्यासकारों की लोकतंत्रत्मक दृष्टियां तो दूसरी तरफ गांवों से कच्च माल ले जानेवाला अंगरेजी लूट-तंत्र. इसी तरह राज में दो प्रतिशत अंगरेजी जाननेवालों का ‘प्रभु वर्ग’ बन गया. अपनी सुशासन व्यवस्था और सभ्यता के दावों के बावजूद अंगरेजी राज का शासक-चरित्र साफ-साफ नजर आने लगा. तभी यह भी नजर आने लगा कि विषमता और शोषण की इन दरारों के अधिकाधिक फैलते जाने का एक मुख्य कारण विदेशी भाषा है, जिसने ‘अमीर हिंदुस्तान’ और ‘गरीब हिंदुस्तान’ बना दिये हैं. इसे समझते हुए ‘स्वराज्य’ की मांग कर रहे गांधीजी ने उसे ही ‘राष्ट्रभक्त’ कहा और उसके लक्षणों में सबसे पहले नंबर पर रखा ‘जो अंगरेजी भाषा का उपयोग लाचारी से करेगा.’ यह उल्लेख ‘हिंद स्वराज’ के आखिरी 20वें अध्याय में है.
आजादी के बाद भी अंगरेजी के आतंक से मुक्त होने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, बल्कि उसे एक दुराग्रही संकीर्ण ‘भाषा विवाद’ में बदल दिया गया. अंगरेजी की दासता से मुक्त होने के बजाय इसे हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच प्रतिस्पर्धा व प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया गया.