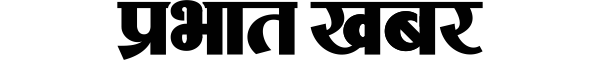भीषण जल संकट की ओर बढ़ता देश
रोज नहाया तो जुर्माना देना पड़ेगा, यह एक पंचायत का फैसला है. जेठ की जलती दुपहरी में जब चढ़ता पारा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काल बन रहा है, रोज न नहाने का फैसला झारखंड के प्रखंड सगमा के कटहर कला गांव के लोगों पर लागू है. पहली नजर में पंचायत का यह फैसला ‘तुगलकी […]
रोज नहाया तो जुर्माना देना पड़ेगा, यह एक पंचायत का फैसला है. जेठ की जलती दुपहरी में जब चढ़ता पारा रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काल बन रहा है, रोज न नहाने का फैसला झारखंड के प्रखंड सगमा के कटहर कला गांव के लोगों पर लागू है. पहली नजर में पंचायत का यह फैसला ‘तुगलकी फरमान’ जान पड़ता है, पर गांव के पश्चिम टोले की पंचायत और करे भी तो क्या! आदिवासी समुदाय के 80 घर, लेकिन बस्ती में बस दो ही चापानल! आसपास नदी-तालाब, झील-झरना कुछ भी नहीं. दो चापानल से ही नहाना-धोना, खाना-पीना, मवेशियों को पानी, सबकुछ चल रहा है. भीड़ इतनी कि चापानल पर कतार में सुबह लगो तो नल का हत्था दोपहर में हाथ आये. रोज-रोज के झगड़े और मारपीट की नौबत से निपटने के लिए पंचायत को यह फैसला सुनाना पड़ा. तो क्या पंचायत के इस फैसले की गूंज झारखंड सरकार को सुनायी देगी?
झारखंड में सरकार नयी हो या पुरानी, पेयजल की समस्या को उसने घरों में पानी पहुंचाने की प्रशासनिक समस्या के रूप में सोचा है. यह सोच मान कर चलती है कि पानी सरीखा प्राकृतिक संसाधन तो अकूत है, जितनी मर्जी उतना बरतो, घटेगा ही नहीं. पानी की समस्या को सरकार जल संसाधन के बचत और संरक्षण-संवर्धन के हिसाब से सोचती, तो उसे पंचायत के फरमान से पहले झारखंड में कटते पहाड़ों की आवाज सुनायी देती, सिकुड़ते वन-क्षेत्र की फिक्र होती. पहाड़ काट लिये गये, सरकार बेखबर रही. जबकि झारखंड के जनजीवन से बेहतर कौन जानता होगा कि हर झील की एक घाटी होती है, हर घाटी का एक पहाड़ और पहाड़ों पर पसरे जंगल ही बचा कर रखते हैं पानी के वे सोते, जो मनुष्य से लेकर मवेशी तक के जीवन का आधार साबित होते हैं.
कटहर कला से दिल्ली का संगम विहार सैकड़ों मील दूर है, लेकिन वहां भी हालत बहुत अलग नहीं है. हालांकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, जो सबको जरूरत भर मुफ्त पानी देने के वायदे से बनी है, इलाके का विधायक भी सत्ताधारी पार्टी का ही है, तो भी संगम विहार के लोग झुलसाती गरमी में पानी के लिए तरस रहे हैं. विधायक के ऑफिस के सामने ढाई-तीन सौ लोग रोज जमा होते हैं, पानी के टैंकर के लिए. कुछ घरों में एक कमरा आदमियों के लिए है, तो एक पानी की टंकियां रखने के लिए. टंकियां जितनी ज्यादा होंगी, पानी उतना ज्यादा जमा हो सकेगा. यह युक्ति व्यावहारिक है, क्योंकि संगम विहार के लोगों को पता नहीं होता कि अगली दफे कितने दिन बाद पानी के दर्शन होंगे! इस तरह झारखंड के कटहर कला से लेकर दिल्ली के संगम विहार तक, यानी देश के कई हिस्सों में हर साल गर्मियों में पानी के लिए छीना-झपटी मचती है और झगड़ों में लोगों की जान भी चली जाती है. सरकारें कभी आश्वासन देती हैं, तो कभी बहाने बनाती हैं. कहीं कहा जाता है कॉलोनी ही अवैध है, तो कहीं यह कि नलकूप का पैसा दिया था, बिचौलियों ने भ्रष्टाचार किया या गांव के लोग चापानल उखाड़ ले गये. अकसर सरकारें अपना जिम्मा दूसरी सरकारों पर भी डाल देती हैं. जैसे, दिल्ली में पानी नहीं आया तो हरियाणा की सरकार दोषी है, क्योंकि उसने नदी का पानी छोड़ने से मना कर दिया है.
जरा ठहर कर सोचें तो असल समस्या बढ़ती आबादी के बीच पानी के समतामूलक बंटवारे की है. कुछ बरस पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में खेती, उद्योग और घरेलू उपयोग के मद में करीब 829 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्रतिवर्ष खर्च होता है. 2050 तक आबादी, आर्थिक-वृद्धि एवं मध्य-वर्ग के आकार के हिसाब से पानी की मांग दोगुनी से ज्यादा बढ़ जायेगी. पेयजल की मांग देश में पानी की कुल मांग का सिर्फ 4-6 फीसदी है, 90 फीसदी से अधिक मांग खेती व उद्योगों के लिए है. हरित क्रांति से प्रभावित सिंचाई-प्रधान खेती ने जहां देश में भू-जल का स्तर घटाया है, वहीं औद्योगिक व शहरी कचरे ने नदी जल को दूषित कर दिया है. हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत पानी के संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में पानी का युक्तिसंगत व समतामूलक वितरण ही रास्ता हो सकता है. मसलन, दिल्ली में पांचसितारा होटल का एक कमरा प्रतिदिन 1600 लीटर पानी खर्च करता है, वीआइपी आवासों में रोज 30,000 लीटर पानी खपता है, जबकि 78 फीसदी आबादी को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 से 90 लीटर पानी में गुजारा करना पड़ता है. जाहिर है, देश में जरूरत ऐसी जल-नीति और उस पर अमल की है, जिससे कटहर कला या संगम विहार जैसे इलाकों के लोगों के हिस्से का पानी वीआइपी, महंगे होटलों या खेतों-उद्योगों को न मिले, साथ ही उपलब्ध जल-स्नेतों का निरंतर संरक्षण और संवर्धन होता रहे.