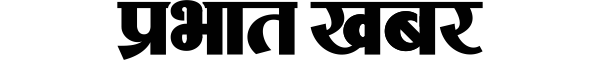उच्च शिक्षा का अंधेरा कोना
बात जब देश में उच्च शिक्षा की स्थिति पर होती है, तब अक्सर इसका मूल्यांकन विश्वविद्यालयों की संख्या, शिक्षक-छात्र अनुपात, बजटीय आवंटन के मानकों पर होता है. ऐसा करते हुए हम उच्च शिक्षा के एक अंधेरे कोने से दूर रह जाते हैं. उच्च शिक्षा का स्तर वास्तव में तय होता है उन शिक्षकों से, जो […]
बात जब देश में उच्च शिक्षा की स्थिति पर होती है, तब अक्सर इसका मूल्यांकन विश्वविद्यालयों की संख्या, शिक्षक-छात्र अनुपात, बजटीय आवंटन के मानकों पर होता है. ऐसा करते हुए हम उच्च शिक्षा के एक अंधेरे कोने से दूर रह जाते हैं. उच्च शिक्षा का स्तर वास्तव में तय होता है उन शिक्षकों से, जो शिक्षा के केंद्रों को बहस-मुहाबिसों, ज्ञान-विज्ञान और नयी चेतना का केंद्र बनाते हैं.
क्या भारत में उच्च शिक्षा की बागडोर ऐसे कुशल हाथों में है? एक अंगरेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा को ‘कांट्रैक्ट’ (अनुबंध) और ‘टेम्पररी’ (अस्थायी) की बैसाखी के भरोसे छोड़ दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 9.33 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से करीब 40 फीसदी शिक्षक कांट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या वैसे लोगों की है, जिनके पास न पीएचडी की डिग्री है, न एमफिल की. न ही उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (नेट) ही उत्तीर्ण की है. सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ये कांट्रैक्ट शिक्षक अमूमन असंतोषजनक सेवा शर्तो पर काम कर रहे हैं. इन्हें औसतन चार से बीस हजार तक के वेतन पर ‘जरूरत और मांग’ के हिसाब से रखा जा रहा है.
इन्हें न भविष्य निधि की सुविधा मिल रही है, न स्वास्थ्य बीमा की. अपने अनुबंध के पुनर्नवीकरण के लिए ये पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन की दया पर निर्भर हैं. और यह कहानी किसी एक राज्य या विश्वविद्यालय की नहीं है. दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भी कांट्रैक्ट का चलन जोरों पर है. मिसाल के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय (दिविवि) के पोस्ट ग्रेजुएट विभागों के करीब आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. दिविवि के विधि संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर के 100 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 12 पर स्थायी शिक्षक काम कर रहे हैं. जाहिर है, इन विश्वविद्यालयों की गाड़ी अस्थायी नियुक्तियों के भरोसे चल रही है. यह एक माना हुआ तथ्य है कि शिक्षा परिसरों में स्थायी शिक्षकों के पास ही छात्र निर्माण के दीर्घकालीन लक्ष्य पर काम करने का, छात्रों से संवाद करने का मौका होता है. खुद अपने भविष्य को लेकर संशय में घिरे शिक्षक से छात्रों के भविष्य निर्माण की अपेक्षा करना बेमानी है. शायद यह हमारी प्राथमिकता में भी नहीं है.