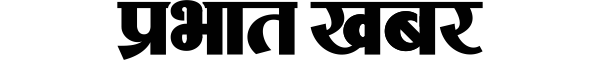विकास के नाम पर राज्य की लूट!
आकार पटेल वरिष्ठ पत्रकार दस साल पहले, 2006 में, लता मंगेशकर ने घोषणा की थी कि अगर मुंबई के पेडर रोड पर स्थित उनके भवन के सामने फ्लाइओवर बनेगा, तो वह भारत छोड़ कर चली जायेंगी. पहले उन्होंने कहा कि इससे उनकी आवाज पर असर पड़ेगा, और बाद में तर्क दिया कि अगर सड़क पर […]
आकार पटेल
वरिष्ठ पत्रकार
दस साल पहले, 2006 में, लता मंगेशकर ने घोषणा की थी कि अगर मुंबई के पेडर रोड पर स्थित उनके भवन के सामने फ्लाइओवर बनेगा, तो वह भारत छोड़ कर चली जायेंगी. पहले उन्होंने कहा कि इससे उनकी आवाज पर असर पड़ेगा, और बाद में तर्क दिया कि अगर सड़क पर खुदाई की गयी, तो कई इमारतों की नींव हिल जायेगी. बहरहाल, वह फ्लाइओवर नहीं बना.
इस सप्ताह मुझे भारत में कोयला खदानों के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं. इससे आपको कुछ बातों का पता चल सकेगा कि विकास की महान परियोजना किस तरह चल रही है. यह जानकारी मुझे मेरी सहयोगी अरुणा चंद्रशेखर की रिपोर्ट से मिली है, जिस पर वह काम कर रही हैं.
सबसे पहले खदानों के नियमन के कानूनों पर नजर डालते हैं, जो भारतीय नागरिकों की संपत्ति और अधिकारों की सुरक्षा करती हैं. वर्ष 2014 में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन कानून में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार मिला था. इसमें प्रावधान है कि ‘जहां सार्वजनिक-निजी सहभागिता की परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है वहां प्रभावित परिवारों में से 70 फीसदी की सहमति आवश्यक है, और निजी परियोजनाओं के लिए 80 फीसदी परिवारों की सहमति आवश्यक है.’ यह मुझे उचित प्रतीत होता है.
इस कानून में भूमि के अधिग्रहण से पहले अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की पूर्व अनुमति का भी प्रावधान है. इसके अलावा, इसमें ‘सामाजिक प्रभाव का आकलन’ भी शामिल है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्रभावित समुदायों के साथ मिल कर परियोजना के लोगों की भूमि और आजीविका पर प्रभाव, तथा इसके आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन.
अगर आपको लगता है कि यह सही है, तो आपको यह जानना चाहिए कि यह कानून उन जमीनों के लिए लागू नहीं होता है, जिन्हें कोयला खदानों के लिए लिया गया है. विशेष रूप से भूमि के मालिकों से कोई मंजूरी नहीं ली जाती है, जमीन लेने से पहले उनकी सहमति जरूरी नहीं होती है और इसके सामाजिक प्रभाव के आकलन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता.
प्रभाव के एक छोटे पहलू के बारे में जानना पाठकों को दिलचस्प लगेगा, खास कर लता मंगेशकर के विरोध को पढ़ने के बाद, जिसे चंद्रशेखर ने रेखांकित किया है. खदानवाले इलाकों में शाम तीन से चार बजे के बीच विद्यालय बंद रखे जाते हैं, क्योंकि विस्फोट इतने भयानक होते हैं कि विद्यालयों के भवन कांपने लगते हैं.
अब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम पर विचार करें. यह कानून ‘वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासी समुदायों के भूमि एवं अन्य संसाधनों पर परंपरागत अधिकारों को मान्यता देता है. इन समुदायों के सदस्य उस वन-भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार का दावा कर सकते हैं, जिस पर वे निर्भर हैं या जिसे उन्होंने कृषियोग्य बनाया है.
समुदाय सामान्य संपत्ति संसाधनों पर अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं, जिनमें सामुदायिक या ग्राम वन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थान, और जल निकाय शामिल हैं.’ यह कानून कहता है कि वन संपदा पर अधिकार के निर्धारण में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए. यह सब बहुत अच्छा है. लेकिन, दुर्भाग्यवश, खुद आदिवासी मामलों का मंत्रालय मानता है कि सरकार ने इस कानून की बहुधा अवहेलना ही की है.
भूमि अधिग्रहण के नियमन से संबंधित एक अन्य कानून है- पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार कानून. इसे पेसा (पीइएसए) भी कहा जाता है. इसमें प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करने से पहले तथा ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन से पंचायतों से सलाह करना जरूरी है. सरकार ने इस कानून की भी कमोबेश अवहेलना ही की है.
एक अन्य कानून पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम है, जिसमें एक निर्धारित आकार की सभी परियोजनाओं को संभावित रूप से प्रभावित होनेवाले स्थानीय समुदायों की जन-सुनवाई के बाद पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेना जरूरी है. चंद्रशेखर बताती हैं कि कानूनन जरूरी सामाजिक प्रभाव आकलन को ‘करीब-करीब कभी पूरा नहीं किया जाता है.’ इसका एक कारण है कि आकलन की सत्यता और पूर्णता के मूल्यांकन की जिम्मेवारी सरकार की नहीं है.
एक कानून ऐसा भी है, जिसका सरकार बहुत अच्छी तरह पालन करती है और लागू करती है, जिसके तहत वह भूमि पर कब्जा करती है. यह कानून है- कोयला संपन्न क्षेत्र अधिनियम. इसके तहत सरकार अपने गजट में एक आदेश प्रकाशित करती है (आखिरी बार आपने कोई सरकारी गजट कब पढ़ा था?). और फिर, अगर 30 दिनों के भीतर कोई लिखित आपत्ति दर्ज नहीं करायी जाती है, तो वह प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है जिसके तहत वह भूमि ‘पूरी तरह से केंद्र सरकार की संपत्ति (बिना किसी अवरोध के)’ बन जाती है.
कोल इंडिया लिमिटेड (जो देश की कुल खदान कार्यों के दो-तिहाई हिस्से को नियंत्रित करती है) की नीतियों को परखने के बाद एक संसदीय समिति ने कहा था कि आदिवासी समुदायों की ‘शायद ही कोई पहुंच आधिकारिक गजट तक है, जो वे देख सकें कि उनकी भूमि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जा रही है.’
मेरा मानना है कि यह सब वास्तव में पूरी तरह जान-बूझकर किया जाता है. इस देश में औद्योगिक विकास आदिवासियों की जमीन को लूट कर किया जा रहा है. (रविवार, छह फरवरी को खबर आयी थी कि झारखंड में अदानी द्वारा कोयला से चलनेवाला दो बिलियन डॉलर का विद्युत संयत्र स्थापित किया जा रहा है.) और, हम मध्य वर्ग के लोग इस लूट में पूरी तरह से शामिल हैं.हममें से कौन विकास के लिए अपना फ्लैट त्याग देगा? हमारा अभिजात्य बहुत जरूरी फ्लाइओवर के निर्माण को रोक सकता है.
हमारा जोर इस बात पर है कि जो लोग अनिच्छुक हैं, पर कमजोर भी हैं, वे ही सारा बलिदान करें और उसके बाद जब राज्य के विरुद्ध हिंसा होती है, तब हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं. जमीन के कब्जे की इस खुलेआम लूट की हकीकत जान लेने के बाद ‘माओवादी’ और निश्चित रूप से ‘विकास’ जैसे शब्दों के बिल्कुल अलग मतलब निकलते हैं.