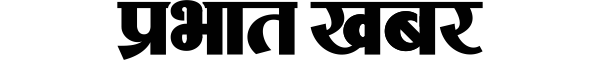सूखे की मार, हम जिम्मेवार
डॉ भरत झुनझुनवाला अर्थशास्त्री देश के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं. भूमिगत जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है. आलम यह है कि समर्थवान अंगूर व मिर्च की खेती कर रहे हैं, जबकि सामान्य किसान पीने के पानी को भी तरस रहे हैं. साठ के दशक में हरित क्रांति के साथ-साथ देश में […]
डॉ भरत झुनझुनवाला
अर्थशास्त्री
देश के कई हिस्से सूखे की चपेट में हैं. भूमिगत जलस्तर तेजी से नीचे गिर रहा है. आलम यह है कि समर्थवान अंगूर व मिर्च की खेती कर रहे हैं, जबकि सामान्य किसान पीने के पानी को भी तरस रहे हैं. साठ के दशक में हरित क्रांति के साथ-साथ देश में ट्यूबवेल से सिंचाई का विस्तार हुआ. गंगा के मैदानी इलाके में पहले भूमिगत जल-स्तर बरसात में 5-6 फुट और गर्मी में 15-20 फुट रहा करता था. 20 फुट के नीचे की धरती पानी से लबालब भरी रहती थी. बरसात के समय जितना पानी इस भूमिगत तालाब में समाता था, उतना पानी जाड़े और गर्मी में निकाल कर सिंचाई की जाती थी.
ट्यूबवेल की तकनीक ने परिस्थिति में मौलिक बदलाव आया. 200 फुट क्या, कहीं-कहीं 500 फुट तक धरती के तालाब में पड़े पानी को खींच लिया गया है. धरती के पानी का जलस्तर गिर गया है. अब बरसात में पानी 500 फुट नीचे जाकर ठहरता है. जिन किसानों के ट्यूबवेल इस गहराई से पानी निकालने में सक्षम होते हैं, उनके खेत हरे रहते हैं. शेष के ट्यूबवेल सूख जाते हैं. पानी उतना ही है. पहले वह 20 फुट पर ठहरता था और निकाल लिया जाता था और अब वह 500 फुट पर ठहरता है और निकाल लिया जाता है. उतने ही पानी को निकालने के लिए हर किसान 500 फुट से पानी खींचने की बिजली जला रहा है.
पानी का जल-स्तर गिरने से धरती में अब तक सुप्त पड़े हानिकारक तत्व जागृत हो उठे हैं. बिहार तथा बंगाल की धरती में नीचे आरसेनिक भारी मात्रा में जमा है. पानी के नीचे से निकाले जाने के कारण रिस रहे नीचे पानी तथा आरसेनिक के बीच रगड़ उत्पन्न हो रही है. इस पानी में आरसेनिक मौजूद है.
यह जन-स्वास्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है. पीने के पानी से आरसेनिक को निकालने के लिए घरों में आरओ लगाना पड़ रहा है. तटवर्ती क्षेत्रों में एक और समस्या है. पहले बरसात का मीठा पानी 20 फुट तक भरा रहता था. समुद्र के खारे पानी को वह अंदर नहीं आने देता था. अब धरती के नीचे के पानी को ट्यूबवेल से निकाल लिया गया है और समुद्र का खारा पानी धरती के तालाबों में भर गया है. इससे पानी की स्थायी उपलब्धता घटी है. सूखा नयी बात नहीं है. समस्या यह है कि सूखे के समय जीवन निर्वाह करने के लिए अब पानी उपलब्ध नहीं है, चूंकि हमने भूमिगत तालाबों को सुखा दिया है.
संविधान में पानी का विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है. केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि नये ट्यूबवेल लगाने के लिए लाइसेंस प्रणाली को लागू करें. कुछ राज्यों द्वारा इस प्रकार के कानून बनाये भी गये हैं, परंतु स्थानीय क्षत्रपों के प्रभाव से इसे लागू नहीं किया जा रहा है. लागू हो जाये तो भी विशेष लाभ नहीं होगा, चूंकि वर्तमान में लगे हुए ट्यूबवेलों से भूमिगत तालाबों का अति दोहन जारी रहेगा.
उपाय है कि हर क्षेत्र में ट्यूबवेल की अधिकतम गहराई को कानूनी स्तर पर निर्धारित कर दिया जाये. मान लीजिए, किसी क्षेत्र में अधिकतम गहराई को 100 फुट निर्धारित कर दिया गया. क्षेत्र में वर्तमान में तमाम ट्यूबवेल 200, 300, 500 फुट गहरे हैं. इन्हें निकाल कर इनकी पाइपों एवं तार को छोटा कर दिया जाये, जिससे आनेवाले समय में ये 100 फुट से नीचे का पानी न निकाल सकें. 500 फुट से 100 फुट की गहराई में पानी का पुर्नभरण होगा. बरसात का पानी रिस कर इस गहराई में समा जायेगा और निकाला नहीं जा सकेगा. लेकिन कुछ समय बाद बाकी ट्यूबवेलों को 100 फुट पर पानी उपलब्ध हो जायेगा.
दूसरा उपाय है कि अधिक मात्रा में सिंचाई मांगनेवाली फसलों पर क्षेत्रवार प्रतिबंध लगा दिया जाये. किसान द्वारा पानी की खपत को कम करना होगा. सरकार को चाहिए कि हर ब्लाॅक में पड़नेवाली वर्षा की गणित करे और देखे कि उतनी वर्षा में उस ब्लाॅक में किन फसलों की खेती सुगमता से हो सकती है.
शेष फसलों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया जाये. इस तरह किसान की पानी की मांग कम हो जायेगी और भूमिगत जल के अतिदोहन में सहज ही रुकावट आयेगी.
वर्षा के पानी के पुनर्भरण के लिए भी योजना बनानी चाहिए. बरसात के पानी का भाखड़ा और टिहरी संग्रहण करने से कई नुकसान होते हैं. डैम में पानी रोक लेने से डैम के नीचे के क्षेत्र में भूमिगत जल-स्तर गिरता है और यहां सिंचाई में गिरावट आती है. जैसे हथिनीकुंड से सोनीपत तक यमुना के किनारे खेती कम हो रही है, चूंकि हथिनीकुंड से पानी को निकाल कर कमांड एरिया में पहुंचाया जा रहा है. सिंचाई का विस्तार कम ही हो रहा है. केवल सिंचाई के स्थान में परिवर्तन हो रहा है. वर्तमान सूखा आंशिक रूप से ही प्राकृतिक है, इसे बनाने में हमारा योगदान ज्यादा है. हमें अपनी जल-नीतियों को दुरुस्त करना होगा.