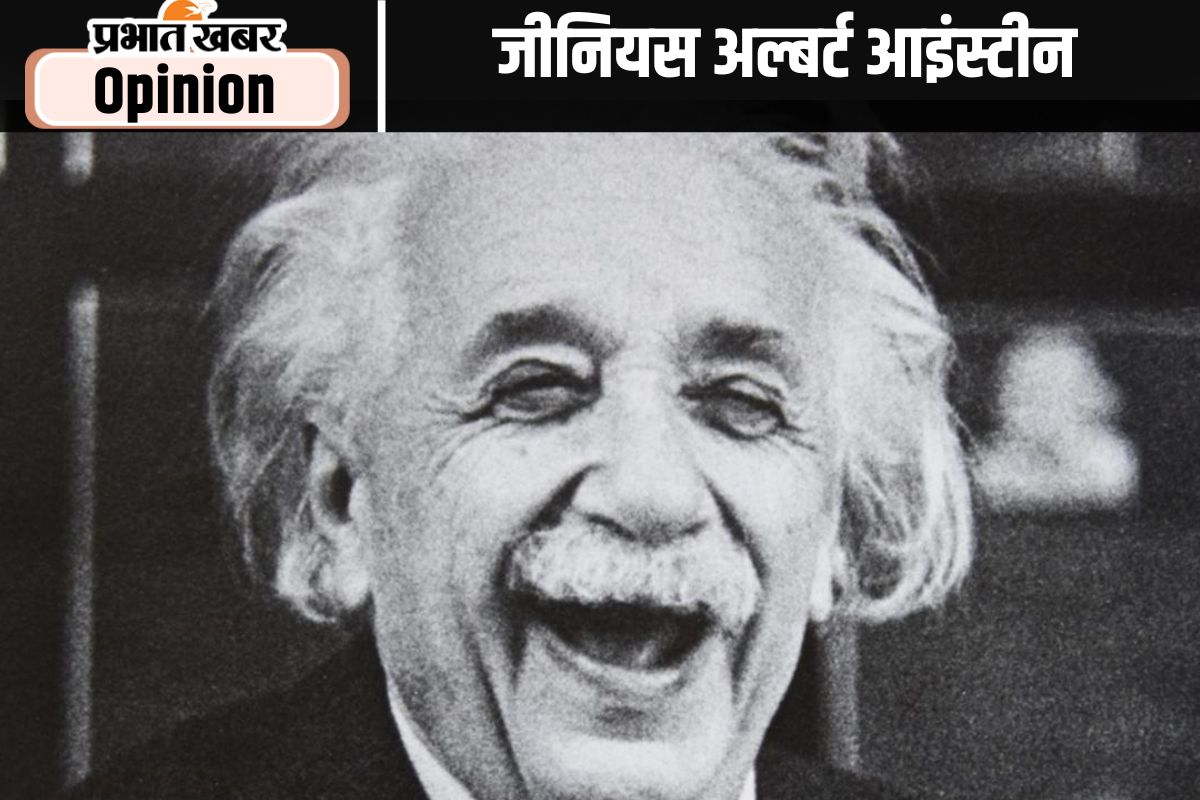Albert Einstein : महानतम वैज्ञानिक, गणितज्ञ व दार्शनिक अल्बर्ट आइंस्टीन का (दुनिया के अधिकतर देशों में जिनकी जयंती ‘जीनियस डे’ के रूप में मनायी जाती है) हमारे देश से रिश्ता इस मायने में कुछ ज्यादा ही प्रगाढ़ है कि वह महात्मा गांधी के मुक्त कंठ प्रशंसक थे. उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यह मानने में कठिनाई होगी कि महात्मा जैसा हाड़-मांस का कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर आया था.
वर्ष 1879 में आज के ही दिन जर्मनी में जन्म के बाद निरंतर चिंतन-मनन और शोध की मार्फत उन्होंने विज्ञान की दुनिया को ऐसे सिद्धांत दिये, जिन्होंने उसकी दशा व दिशा तो बदल ही डाली, ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को भी कल्पना से परे बढ़ा दिया. उनकी कई समाजशास्त्रीय स्थापनाएं भी उनकी पहचान का हिस्सा हैं. जैसे, उनका मानना था कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है. ज्ञान सीमित है, जबकि कल्पना दुनिया को घेर लेती है… दुनिया के बारे में सबसे अबूझ बात यह है कि यह समझने योग्य है… प्रतिभा और मूर्खता के बीच अंतर यह है कि प्रतिभा की अपनी सीमाएं होती हैं, जबकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती… हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच से नहीं कर सकते, जिस सोच का प्रयोग हमने उन्हें खड़ी करते समय किया था. आइंस्टीन ने कभी अपने जीनियस होने का अहंकार नहीं पाला. उन्होंने कहा था, ‘मुझे अपने व्यक्तित्व में जीनियस होने का इसके अलावा कोई लक्षण नजर नहीं आता कि मैं अपनी समस्याओं के साथ उनके समाधान के लिए अधीर हुए बगैर अपेक्षाकृत ज्यादा देर तक बना रहता हूं. मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए एक घंटा होता है, तो मैं 55 मिनट उसके बारे में और पांच मिनट समाधान के बारे में सोचने में बिताता हूं, और कोई भी ऐसा करके जीनियस हो सकता है.’
जीनियस कहलाने वालों के बारे में आम धारणा है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है. पर आइंस्टीन बहुत भुलक्कड़ थे. इतने कि एक बार ट्रेन में यात्रा के दौरान वह इसलिए टिकट परीक्षक को अपना टिकट नहीं दिखा पाये थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने उसे कहां रख दिया है. उन्हें टिकट खोजने में बेचैन देख टिकट परीक्षक ने कहा कि कोई बात नहीं, वह उन्हें अच्छी तरह पहचानता है और उसे विश्वास है कि उन्होंने टिकट जरूर खरीदा होगा. इस पर उनका भोला-सा सवाल था, ‘टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं?’ भुलक्कड़ी की हद यह थी कि वह लोगों के फोन नंबर तक भूल जाते थे, यहां तक कि अपना फोन नंबर भी. एक बार किसी ने इस पर आश्चर्य जताया, तो उन्होंने यह कहा कि मैं कोई ऐसी चीज क्यों याद रखूं, जो किताब या नोटबुक में ढूंढने पर मिल जाती है.
एक दिन प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से, जहां वह कार्यरत थे, लौटते हुए वह टैक्सी में बैठे, तो घर का ही पता भूल गये. टैक्सी के अपरिचित ड्राइवर से उन्होंने पूछा कि क्या उसे आइंस्टीन का घर मालूम है? ड्राइवर का उत्तर था : उनका घर भला कौन नहीं जानेगा? आप चाहें तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं. तब उन्होंने उसे बताया कि वही आइंस्टीन हैं और अपने घर का पता भूल गये हैं. इस पर आश्चर्यचकित ड्राइवर ने उन्हें उनके घर तो पहुंचाया, पर उनके बार-बार कहने के बावजूद किराया नहीं लिया. सरल जीवनशैली और वेशभूषा भी उनकी एक विशेषता थी. एक बार उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वह ढंग के कपड़े पहन यूनिवर्सिटी जाया करें. इस पर उनका उत्तर था, ‘वहां बन-ठन कर भला क्या जाना, वहां तो सब वैसे भी जानते हैं कि मैं कौन और क्या हूं.’ लेकिन अपने पहले बड़े सम्मेलन में जाने से पहले पत्नी ने जब उनसे अच्छे कपड़े पहन लेने को कहा, तो उनका जवाब था, ‘क्या फायदा, वहां कौन मुझे जानने वाला बैठा है?’
बचपन में पढ़ाई-लिखाई में उनका हाल इतना बेहाल था कि गणित के शिक्षक ने उनके फिसड्डी होने को लेकर उन्हें ‘लेजी डॉग’ तक कह डाला था. कई अन्य लोग भी इस कमजोरी को लेकर उनका मजाक उड़ाया करते थे. जब वह सत्रह साल के थे, तब एक कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में गणित व विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में बुरी तरह फेल हो गये थे. लेकिन जब अध्ययन के प्रति अपनी लगन को जगाने में वह सफल हो गये, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. विज्ञान और गणित की परीक्षाओं में तो खैर वह कभी विफल नहीं हुए. उनकी दूरदर्शी वैज्ञानिक प्रतिभा का एक बड़ा उदाहरण यह भी है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के वक्त से पहले ही मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर को लेकर वह चिंतित थे. उन्हें डर था कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब प्रौद्योगिकी हमारी मानवीय अंतःक्रिया को पीछे छोड़ देगी और दुनिया में मूर्खों की एक पीढ़ी होगी. (ये लेखक के निजी विचार हैं.)