स्थानीय भाषा बोध और संप्रेषणीयता
उदारीकरण के तीक्ष्ण विस्तार के दौर में जब बाजार ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनानी शुरू की, तो पत्रकारिता ने इसमें भी अपने विस्तार की उम्मीद खोज ली.
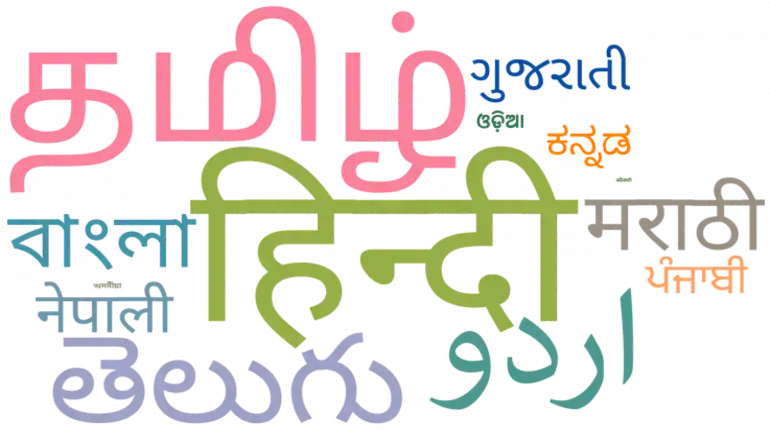
आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई, पर इसने 20वीं सदी के शुरूआती वर्षों में स्तरीयता के संदर्भ में एक मानक स्तर हासिल कर लिया. इसी दौर में हिंदी राष्ट्रीय होने की ओर बढ़ती है और इसमें भावी बहुभाषी स्वतंत्र भारत की भाषाओं के बीच सेतु के तौर पर देखा जाता है. ब्रिटिश भारतविद् फ्रांचेस्का आर्सिनी इसी दौर की हिंदी को समूचे भारतीय राष्ट्र के मूल्यों का लोकवृत्त रचयिता के तौर पर देखती हैं.
अमृत राय इसी दौर में हिंदी में राष्ट्रवाद के बीज भी देखते हैं. लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी नये रूप में सामने आती है. विशेषकर हिंदी पत्रकारिता स्थानीयता की ओर उन्मुख होती है और राष्ट्रीय से स्थानीय होने की इस यात्रा में वह स्थानीय भाषाओं के तमाम शब्दों को न सिर्फ स्वीकार करती है, बल्कि उन्हें अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ढालकर स्थानीय संपर्क का जीवंत माध्यम बन जाती है.
एक व्याख्यान में अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक ईएम फास्टर ने कहा है कि वैश्विक होने के लिए स्थानीय होना जरूरी है. उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, वही वैश्विक स्तर पर प्रभावकारी हो सकता है. फास्टर ने जब यह प्रस्थापना दी थी, तब वैश्वीकरण का दौर नहीं था. भारत में उदारीकरण के बाद जिस वैश्विक ग्राम की कल्पना की गयी, उसकी कोई सोच भी नहीं थी. हालांकि भारतीय परंपरा इसे दूसरे रूप में हजारों साल पहले स्वीकार कर चुकी थी.
‘उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम’ की अवधारणा नयी नहीं है. औपनिवेशीकरण से विकसित मानसिक गुलामी की ही वजह से भारतीय बुद्धिजीवियों में एक प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है. उन्हें अपना हर पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक दर्शन जहां दकियानूसी लगता रहा है, वहीं आधुनिकता के नाम पर उसी लोक सांस्कृतिक परंपरा जैसी पश्चिम की अवधारणाएं उसे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक और ग्राह्य लगती रही हैं.
उदारीकरण के तीक्ष्ण विस्तार के दौर में जब बाजार ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बनानी शुरू की, तो पत्रकारिता ने इसमें भी अपने विस्तार की उम्मीद खोज ली. विस्तार की इस प्रक्रिया में उसे स्थानीय समुदायों में अपनी पैठ बनाने का सबसे बेहतर तरीका नजर आया स्थानीय संस्कृति को तवज्जो देना. यही वजह है कि पत्रकारिता में स्थानीय लोकोक्तियों, मुहावरों और शब्दों का प्रयोग बढ़ा है.
हालांकि ऐसा नहीं है कि उदारीकरण के दौर में ही स्थानीयताबोध की पत्रकारिता में स्वीकार्यता बढ़ी. साहित्य में तो इसकी शुरूआत तभी हो गयी थी, जब आचार्य शिवपूजन सहाय ने ‘देहाती दुनिया’ नाम से उपन्यास लिखा. इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है. बाद के दिनों में इसे केशव प्रसाद मिश्र ने अपनी कहानियों से इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया. उनके उपन्यास ‘कोहबर की शर्त’ में लोक की माटी और लोकभाषा की खुशबू महसूस की जा सकती है.
इस प्रक्रिया को उच्च स्तर पर पहुंचाया फणीश्वर नाथ रेणु ने. लोक का तह विस्तार तत्कालीन पत्रकारिता में भी नजर आता है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तब पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हस्तियां ज्यादातर साहित्य की ही शख्सियतें थीं. स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी जो अखबार जनपदों से निकल रहे थे, उनमें भी प्रकाशन और प्रसार क्षेत्रों की भाषिक विशेषता के साथ स्थानीय लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग हो रहा था.
वैसे भी भाषा और संस्कृति की विशेषता उसके नैरंतर्य में ही है. इस आधार पर कहा जा सकता है कि हिंदी पत्रकारिता में स्थानीय बोध की नींव उसके शुरूआती दिनों में ही पड़ गयी थी. अपनी सफलता की गारंटी स्थानीय बोध को हिंदी पत्रकारिता में पहली बार अमर उजाला ने माना. आगरा से शुरू होने वाला यह पहला अखबार था, जिसने स्थानीय बोध को स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश के उन पहाड़ी इलाकों में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की, जिन्हें अब उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है.
वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने एक आलेख में स्वीकार किया है कि हिंदी में स्थानीय बोध को गति देने की प्रेरणा तेलुगू अखबार इनाडु से मिली. हिंदी की पत्रकारिता का जैसे-जैसे विस्तार होता गया है, वैसे-वैसे उसने स्थानीय शब्दों को अपनी अंजुरी में भरकर उसे अपना बना लिया है.
हिंदी के टेलीविजन में स्थानीय शब्दों, खासकर मुहावरों और लोकोक्तियों के इस्तेमाल के जरिये खुद को ज्यादा संप्रेषणीय बनाया है. हिंदी समाचार चैनल अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अपने पांव कुल्हाड़ी मारना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कांटा निकालना, कान पर जूं न रेंगना, दांत खट्टे करना, खिल्ली उड़ाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तिल का ताड़ बनाना, डींग हांकना जैसे तमाम मुहावरों और लोकोक्तियों का उपयोग कर अपनी भाषा को न सिर्फ चुटीला बनाते हैं, बल्कि उसके जरिये आम लोगों के बीच अपनी पैठ और पहुंच भी बढ़ाते हैं.