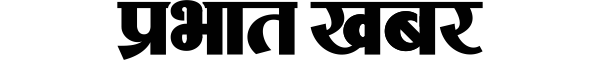प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध हमें आगे आना होगा
plastic waste : कूड़े का बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का है, जो अति सूक्ष्म रूम में हमारे समूचे तंत्र की रक्त शिराओं से लेकर सांस तक के लिए संकट बन चुका है. विशाखापत्तनम से बस्तर को जाने वाले रास्ते पर एक छोटा-सा कस्बा है कोरापुट. चारों तरफ पहाड़ और हरियाली है. जैसे ही बसाहट समाप्त होती है, ऊंचाई का घाट आता है और दोनों तरफ दूर-दूर तक प्लास्टिक की पन्नियां, पानी की बोतलें और नमकीन-चिप्स के पैकेट उड़ते दिखते हैं.
Plastic Waste : पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्थानीय निकायों को ठोस कूड़े के निष्पादन में कोताही बरतने पर नाखुशी जाहिर करते हुए पूछा कि हर दिन 300 टन ठोस कूड़े का निपटान कैसे हो रहा है. दिल्ली देश की सत्ता का केंद्र है, सो यहां कि चिंता जल्दी ही सामने आ जाती है. जबकि यह समस्या पूरे देश की है.
कूड़े का बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का है, जो अति सूक्ष्म रूम में हमारे समूचे तंत्र की रक्त शिराओं से लेकर सांस तक के लिए संकट बन चुका है. विशाखापत्तनम से बस्तर को जाने वाले रास्ते पर एक छोटा-सा कस्बा है कोरापुट. चारों तरफ पहाड़ और हरियाली है. जैसे ही बसाहट समाप्त होती है, ऊंचाई का घाट आता है और दोनों तरफ दूर-दूर तक प्लास्टिक की पन्नियां, पानी की बोतलें और नमकीन-चिप्स के पैकेट उड़ते दिखते हैं. जाहिर है कि जब वहां बरसात होती है, तब इन सभी से उपजा जहर धीरे-धीरे जमीन, खेत में जज्ब होता है, जो अंत में इंसान की जीवन रेखा घटा देता है. कोरापुट तो बानगी है, हर जगह हरियाली से दमकते मैदान, पहाड़ धीरे-धीरे प्लास्टिक कचरे से भरते जा रहे हैं. दिल्ली में तो शीर्ष अदालत कुछ निदान निकलवा देगी, पर उससे कुछ दूर मोदीनगर या पलवल में ऐसा तंत्र नहीं, जो इसकी परवाह करे.
बेशक स्वच्छता अभियान से शौचालय और कचरे के बारे में लोग जागरूक हुए, पर हम पाते हैं कि एक तो घर का कचरा निकाल कर बाहर कर दिया, दूसरा हम कोई ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं कर पाये, जिससे कचरा कम हो और इसका निपटान कारगर हो. जनवरी, 2019 में केंद्र ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी देश में 41.36 लाख टन प्लास्टिक कचरा सालाना पैदा हो रहा है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2018-19 में यह 33.6 लाख टन था, जो 2019-20 में 34.69 लाख टन, 2020-21 में 41.26 लाख टन, 2021-22 में 39.01 लाख टन व 2022-23 में 41.36 लाख टन हो गया.
संसद को यह भी बताया गया कि देशभर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों (पीडब्लूएमयू) की मात्र 978 इकाइयां है. तमिलनाडु में सर्वाधिक 326, आंध्र प्रदेश में 139, बिहार में 102, उत्तर प्रदेश में 68, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में 51-51, केरल में 48, जम्मू-कश्मीर में 43 और तेलंगाना व हिमाचल प्रदेश में 29-29 इकाइयां हैं. जबकि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में प्रावधान है कि प्रत्येक ब्लॉक में पीडब्लूएमयू स्थापित की जाए. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्लास्टिक कचरे के संग्रहण व परिवहन के लिए स्थानीय निकायें और ग्राम पंचायतें अधिकृत हैं, पर उनके पास न तो कर्मचारी हैं, न ही बजट. सो छोटे कस्बे की बात छोड़ें, नगर निगम स्तर पर भी कुछ काम हो नहीं पाया.
कुछ वर्ष पहले केरल के कन्नूर जिले को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाया गया था. सिक्किम के पर्यटन ग्राम लाचेन में भी पर्यटकों को ग्रामीण पानी की बोतल या प्लास्टिक कचरा लाने नहीं देते. प्लास्टिक उत्पादन कच्चे तेल, गैस या कोयले से होता है और कुल प्लास्टिक का करीब 40 फीसदी एक बार इस्तेमाल कर फेंक दिया जाता है. पानी की बोतल, खाद्य उत्पादों के रैपर, पॉलिथीन बैग हमारे पास कुछ घंटों के लिए रहते हैं, फिर सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में डेरा डाल लेते हैं. ये समुद्र, सूर्य की किरण, हवा और लहरों के संपर्क में आकर एक इंच के पांचवें हिस्से से भी छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, फिर यही माइक्रोप्लास्टिक कण हमारे फेफड़ों से लेकर मछली, फल-सब्जी में घुल-मिल रहे हैं. महीन टुकड़ों में विखंडित होकर यह ‘प्लास्टिक माइक्रोफाइबर’ बनाता है, जो जल और हवा के जरिये हमें कैंसर जैसी बीमारी दे जाता है. सच यह है कि प्लास्टिक कचरे का संपूर्ण निपटान संभव नहीं हैं, लेकिन समाज इसका प्रचलन कम कर सकता है.
पहले स्याही वाली कलम होती थी, फिर ऐसे बाल-पेन आये, जिनकी केवल रिफिल बदलती थी. आज यूज एंड थ्रो कलम का चलन है. तीन दशक पहले एक व्यक्ति साल भर में बमुश्किल एक कलम खरीदता था. आज हर आदमी साल में औसतन एक दर्जन कलम इस्तेमाल करता है. शेविंग-किट में पहले स्टील या पीतल का रेजर होता था, जिसमें केवल ब्लेड बदले जाते थे. आज ‘यूज एंड थ्रो’ रेजर ही बाजार में मिलते हैं. कुछ साल पहले तक दूध भी कांच की बोतलों में आता था या लोग अपने बर्तन लेकर डेयरी जाते थे. आज पानी भी बोतलों में मिल रहा है. अनुमानत: पूरे देश में रोज चार करोड़ दूध की थैलियां और दो करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फेंकी जाती हैं. डिस्पोजेबल बरतनों, पॉलीथिन की थैलियों का प्रचलन, पैकिंग, अनेक तरीकों से हम कूड़ा बढ़ा रहे हैं. कानूनन बड़ी कंपनियों को अपने उत्पादों की पैकेजिंग में इस्तेमाल प्लास्टिक का त्वरित निपटारा करना होता है, पर शायद ही यह हो रहा है. पानी की छोटी बोतलों पर रोक के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश का सही तरीके से पालन नहीं हुआ. जाहिर है, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा. (ये लेखक के निजी विचार हैं.)